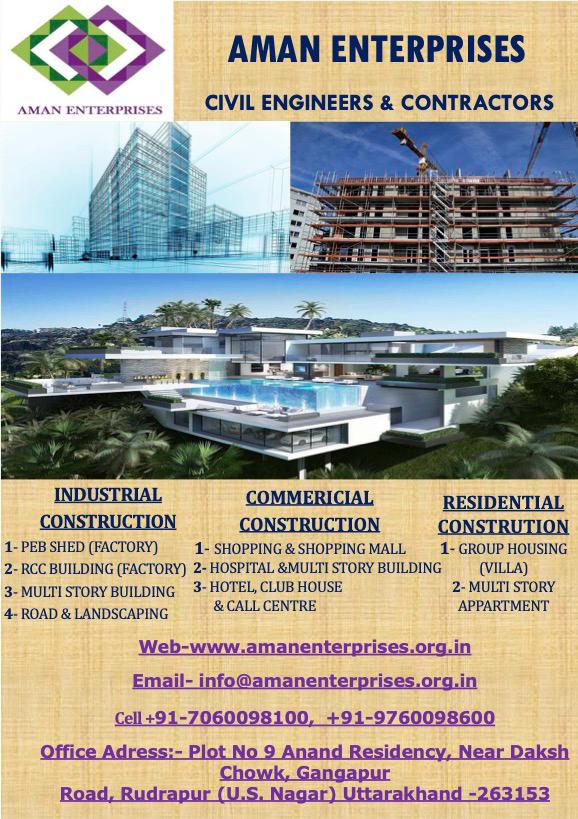देखा जाये तो आधुनिक युद्ध की वास्तविकता अब केवल पारंपरिक टैंकों या मिसाइलों तक सीमित नहीं रही; छोटे आकार के ड्रोन, घूमकर वार करने वाले गोले, रॉकेट और मोर्टार अब अग्रिम मोर्चों से कहीं आगे, सीधे आबादी केंद्रों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में यह निर्णय सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
AK-630 प्रणाली की खासियत इसकी गति और सटीकता में निहित है। 30 मिमी की यह बहु-नलिका तोप प्रति मिनट 3,000 राउंड तक दाग सकती है- जो मूलतः हवा में गोलियों की दीवार खड़ी कर देती है। इसका 4 से 6 किलोमीटर का प्रभावी दायरा सीमित अवश्य है, परंतु इसके उद्देश्य- यानी अंतिम क्षण में आने वाले छोटे या कम ऊँचाई वाले हवाई खतरों को निष्क्रिय करना के लिए यह आदर्श है। इसे ‘क्लोज-इन वेपन सिस्टम’ कहा जाता है और यह नौसेना के युद्धपोतों पर पहले से ही सफलतापूर्वक उपयोग में है। अब इसे स्थल-आधारित, मोबाइल स्वरूप में अपनाना भारतीय थलसेना की वायु रक्षा क्षमताओं में निर्णायक वृद्धि है।
थलसेना, वायुसेना प्रमुख के बयान शब्दों का खेल नहीं, भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक हैं
इस प्रणाली को तेज़ी से तैनात करने की क्षमता, सर्व-कालिक फायर कंट्रोल सिस्टम और “आकाशतीर” वायु रक्षा नेटवर्क में एकीकरण इसे एक आधुनिक, नेटवर्क-संचालित युद्ध प्रणाली का अंग बनाते हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय सेना अब एकीकृत वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली की दिशा में ठोस प्रगति कर रही है, जहाँ विभिन्न स्तरों की रक्षा प्रणालियाँ- लघु, मध्यम और दीर्घ दूरी की समन्वित रूप से कार्य करेंगी।
इस निर्णय की पृष्ठभूमि में हाल ही में शुरू की गई तीन अत्यधिक गतिशील QRSAM (क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल) रेजिमेंटों की खरीद प्रक्रिया भी है, जिसकी लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपये बताई गई है। QRSAM की 30 किमी से अधिक की मारक क्षमता और स्वदेशी विकास इसे भारत की “मेक इन इंडिया” रक्षा नीति का प्रतीक बनाती है। AK-630 जैसे छोटे दायरे के प्रणालियों और QRSAM जैसी मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणालियों का संयोजन भारत को एक “मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क” की दिशा में ले जा रहा है- जो न केवल सीमा क्षेत्रों बल्कि आंतरिक रणनीतिक ठिकानों और शहरी केंद्रों को भी सुरक्षित करेगा।
हम आपको बता दें कि यह पहल ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के बाद अनुमोदित त्वरित खरीद तंत्र के अंतर्गत की जा रही है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान द्वारा तुर्की-निर्मित ड्रोन और चीनी मिसाइलों के समन्वित उपयोग ने भारत के रक्षा विश्लेषकों को यह सिखाया है कि भविष्य का युद्ध न केवल तीव्र होगा, बल्कि अत्यधिक तकनीकी और अप्रत्याशित भी। उस संघर्ष में भारत की मौजूदा बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने प्रभावी भूमिका निभाई थी, परंतु उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि “कम ऊँचाई वाले, तेज़ गति से बदलते हवाई खतरों” से निपटने के लिए नई पीढ़ी की प्रणालियों की आवश्यकता अपरिहार्य है।
AK-630 की तैनाती इस दिशा में एक निर्णायक उत्तर है। इसकी “स्मार्ट फायर” क्षमता- यानी लक्ष्य की गति, दिशा और ऊँचाई के आधार पर स्वचालित समायोजन, आधुनिक वायु रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही सेना की योजना “स्मार्ट और प्रोग्रामेबल गोला-बारूद” को L-70 और ZU-23mm तोपों के लिए अपनाने की है, जिससे पुराने हथियार भी आधुनिक रूप में पुनः उपयोगी हो सकें। यह न केवल तकनीकी दृष्टि से बुद्धिमानी है, बल्कि वित्तीय रूप से भी व्यवहारिक है।
देखा जाये तो भारतीय वायु रक्षा तंत्र अब तीन स्तरों पर सुदृढ़ होता दिखाई दे रहा है। पहला- आकाश, MR-SAM और S-400 जैसी प्रणालियाँ, दूसरा- QRSAM जैसी स्वदेशी मिसाइलें और तीसरा- AK-630, L-70, ZU-23 जैसे त्वरित प्रतिक्रिया तोप तंत्र। देखा जाये तो यह त्रिस्तरीय ढाँचा किसी भी संभावित “स्वार्म अटैक” (झुंड में आने वाले ड्रोन या रॉकेटों के समवेत हमले) के विरुद्ध भारत को एक मजबूत रक्षात्मक कवच प्रदान करेगा।
इसके साथ एक और संकेत स्पष्ट है कि भारत अब “प्रतिक्रिया” नहीं, बल्कि “पूर्व-सक्रिय रक्षा” (proactive defence) के चरण में प्रवेश कर रहा है। तेज़ खरीद, स्वदेशी प्रणालियों पर बल, और नेटवर्क-केंद्रित कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सब मिलकर भारत की रक्षा नीति को एक नये युग में ले जा रहे हैं, जहाँ तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक तत्परता समानांतर रूप से विकसित हो रही हैं।
बहरहाल, यह कहना उचित होगा कि AK-630 जैसी प्रणालियाँ केवल सीमाओं की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक व्यापक सामरिक संदेश हैं कि भारत अब 21वीं सदी के युद्ध-क्षेत्र की चुनौतियों को समझ चुका है और उनके समाधान के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है। यह निर्णय न केवल तत्कालीन खतरों का उत्तर है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के प्रति एक स्पष्ट तैयारी का प्रतीक भी है।