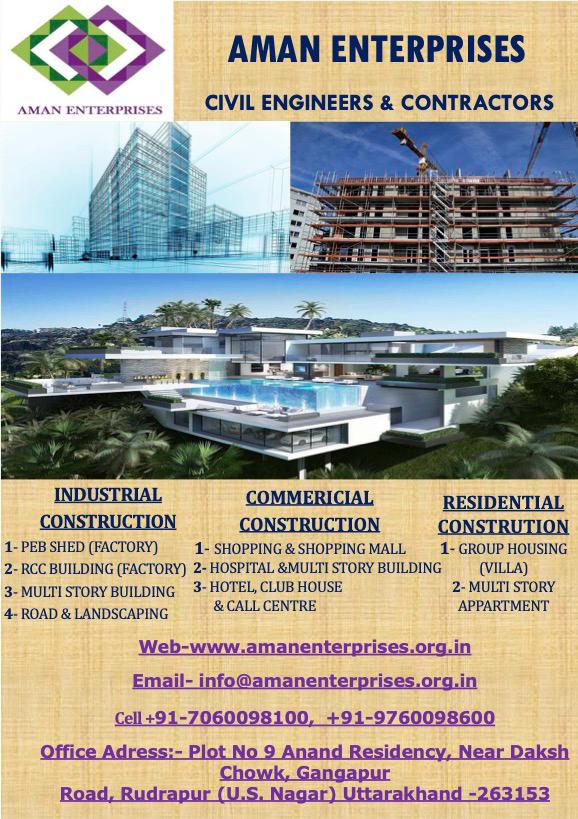संपादकीय: पर्वतीय राज्य की अवधारणा बचाने का एकमात्र रास्ता – क्षेत्रफल आधारित परिसीमन

अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर
संपादक, शैल ग्लोबल टाइम्स / हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी , अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड
उत्तराखंड को जब 2000 में पृथक राज्य का दर्जा मिला, तो इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क था – पहाड़ों की अनदेखी। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक प्राथमिकताओं में पहाड़ी क्षेत्र पिछड़े रहे। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं न मिल पाने के कारण पहाड़ी जनजीवन संघर्षपूर्ण बना रहा। यही पीड़ा उत्तराखंड राज्य आंदोलन की धुरी बनी, और इसी पीड़ा को मिटाने के लिए एक अलग राज्य बना।
लेकिन आज, पच्चीस वर्षों बाद, उसी उत्तराखंड में एक नई चिंता जन्म ले रही है – राजनीतिक असंतुलन। हालिया मतदाता सूचियों के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि राज्य की आबादी का भारी हिस्सा मैदानी जिलों में केंद्रित हो गया है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में मतदाताओं की संख्या पिछले दो दशकों में 72 प्रतिशत तक बढ़ गई, जबकि नौ पर्वतीय जिलों में यह वृद्धि महज 21 प्रतिशत रही। इसका सीधा अर्थ है – पलायन और शहरीकरण की वजह से पर्वतीय जिलों का राजनीतिक वजूद लगातार कमजोर हो रहा है।
यह असंतुलन केवल चुनावी आंकड़ों की बात नहीं है, यह उत्तराखंड की आत्मा पर मंडरा रहा संकट है। अगर भविष्य में परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ, तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा सीटों का अनुपात मैदानी क्षेत्रों के पक्ष में और अधिक झुकेगा। इसका परिणाम यह होगा कि जिन पर्वतीय जिलों के लिए यह राज्य बना था, वे फिर से निर्णय प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।
क्या इसका समाधान है? है – क्षेत्रफल आधारित परिसीमन।
भारत के संविधान में यह गुंजाइश है कि विशेष परिस्थितियों में परिसीमन केवल जनसंख्या के बजाय अन्य आधारों – जैसे भौगोलिक स्थिति, दुर्गमता और क्षेत्रफल – पर भी किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में ऐसा उदाहरण पहले से मौजूद हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की भौगोलिक चुनौतियां, दुर्गमता, सीमांत क्षेत्र और जनसुरक्षा जैसे मसलों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रफल आधारित परिसीमन किया जाना चाहिए।
यह क्यों जरूरी है?
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन: पर्वतीय जिलों की समस्याएं अलग हैं – पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, और संचार की गंभीर समस्याएं आज भी जस की तस हैं। अगर इन क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटता है, तो ये समस्याएं और गहराएंगी।
- राज्य की मूल अवधारणा की रक्षा: उत्तराखंड की परिकल्पना पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी। अगर प्रतिनिधित्व का पलड़ा पूरी तरह मैदान की ओर झुक गया, तो यह राज्य एक बार फिर “पूर्व उत्तर प्रदेश” की तरह बन जाएगा।
- पलायन को रोकने में मदद: यदि पर्वतीय क्षेत्रों को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधन मिलते हैं, तो आजीविका के अवसर पैदा होंगे, और इससे पलायन की दर कम हो सकती है।
सरकार के लिए सुझाव:
- परिसीमन आयोग के गठन से पहले ही राज्य सरकार को संसद और केंद्र सरकार के समक्ष क्षेत्रफल आधारित परिसीमन की मांग मजबूती से रखनी चाहिए।
- जनगणना के आंकड़ों में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों का अलग-अलग वर्गीकरण किया जाए ताकि सटीक और न्यायसंगत विश्लेषण संभव हो।
- पलायन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पर्वतीय जिलों को विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए और इन्हें विशेष विकास सहायता मिले।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के स्थायी साधनों का सृजन कर रिवर्स पलायन को हकीकत में बदला जाए।
राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, और शिक्षाविदों से अपील:
यह सिर्फ एक राजनीतिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है। यह उत्तराखंड के अस्तित्व और उसकी आत्मा से जुड़ा विषय है। सभी जागरूक नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया को इस दिशा में एकजुटता से आवाज उठानी चाहिए। परिसीमन का सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा का है।
यदि हम आज भी चुप रहे, तो कल उत्तराखंड केवल नाम मात्र का पर्वतीय राज्य रह जाएगा – जिसमें न पर्वत बचे होंगे, न पर्वतीय प्रतिनिधित्व।