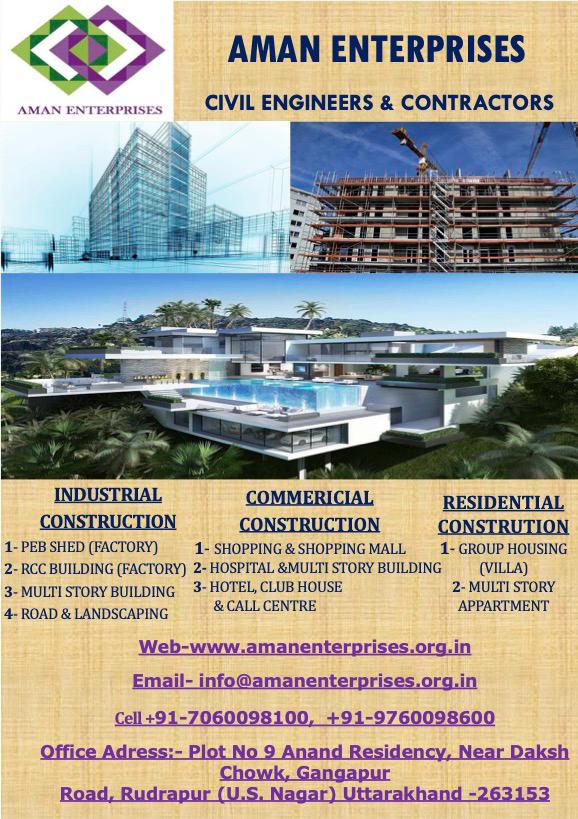कहते हैं, “धरती मां सब कुछ सह लेती है” — लेकिन शायद उत्तराखंड की धरती अब थक चुकी है। यहां विकास की परिभाषा अब पहाड़ काटने, नदियाँ सुखाने और ट्रकों में लदे कंक्रीट से मापी जाती है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘राज्य खनन तत्परता सूचकांक’ जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड को पंजाब और त्रिपुरा के साथ “सी कैटेगरी” में जगह मिली है। यानी, खनन सुधारों के क्षेत्र में राज्य ने कुछ अच्छा किया है — और इसके बदले 100 करोड़ रुपये का इनाम भी मिला है। सुनने में यह खबर किसी उपलब्धि जैसी लगती है, पर असलियत में यह ‘स्वर्ण पदक’ नहीं, बल्कि ‘मिट्टी में मिलते पहाड़ों का प्रमाणपत्र’ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि “खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस” को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब नदियाँ खून की तरह बह रही हैं, जब गाँव के गाँव दरक रहे हैं, जब पहाड़ों के पेट खाली हो रहे हैं — तो आखिर यह ‘सस्टेनेबिलिटी’ किसे कहते हैं?
खनन के नाम पर विनाश की गाथा?उत्तराखंड, जिसे कभी देवभूमि कहा जाता था, अब “डंपरभूमि” में बदल चुका है। खनन की नदियाँ अब देवप्रवाह नहीं रहीं, वे मलबे, डीज़ल और मशीनों की गंध से भर गई हैं।
गंगा की सहायक नदियाँ — कोसी, गौल, दुधिया, ढेला, डोभा, शरदापुर और शारदा — सभी से रेत और बजरी निकालने की होड़ लगी है। इन नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बिगड़ चुका है। पहले जो नदियाँ गर्जना करती थीं, अब वे कराह रही हैं। खनन ने उनका कलेजा खोद दिया है।
यह केवल पर्यावरणीय नुकसान नहीं, बल्कि सामाजिक त्रासदी भी है।
नदियों के किनारे बसे सैकड़ों गाँवों में जमीन धंसने लगी है।
घरों में दरारें हैं, खेतों में फटने लगी मिट्टी है, और पहाड़ों की गोद में भय है।
2023 और 2025 की बारिशों ने जो कहर बरपाया, वह किसी प्राकृतिक नहीं बल्कि “खनन प्रेरित आपदा” थी।
जब नदियों से अंधाधुंध खनन किया जाता है, तो उनकी धारा का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। इससे जल का दबाव बढ़ता है, कटाव तीव्र होता है, और बरसात के मौसम में नदियाँ अपने मार्ग से भटककर गाँवों, खेतों और सड़कों को निगल जाती हैं।
“खनन से विकास” का जो नारा है, वह अब “खनन से विनाश” में बदल चुका है।
कंक्रीट के जंगल और पहाड़ों की चुप्पी,कभी जिस उत्तराखंड की पहचान हरे भरे जंगलों और निर्मल नदियों से थी, अब वह कंक्रीट के पहाड़ों में बदल चुका है।
यह वही कंक्रीट है जो इन्हीं नदियों की रेत से निकली है।
पहाड़ों को काटकर होटल बनाए गए।
नदियों से बजरी निकालकर पुल और हाइवे बने।फिर इन्हीं हाइवे पर ओवरलोड डंपर चले — और उन्होंने सड़कों की सांसें उखाड़ दीं।
आज हालत यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़कों का डामर ओवरलोड डंपरों के नीचे पिघल चुका है। सड़कें जगह-जगह धंस चुकी हैं। गांव की गलियां टूटी हैं। हाईवे पर बने नए पुलों में दरारें पड़ी हैं।
और सबसे दुखद – इन ओवरलोड डंपरों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली।
कितनी ही दुर्घटनाएँ हुईं, लेकिन हर बार मामला “जांच जारी है” कहकर दबा दिया गया।
कभी किसी मंत्री का बयान आया, कभी किसी अधिकारी की “सख्त चेतावनी” — पर जमीनी हालात वही रहे।
ओवरलोड माफिया और मीडिया की मिलीभगत?खनन माफिया और ओवरलोड डंपर संचालक आज उत्तराखंड के सबसे ताकतवर “गैर-राजनीतिक नेता” बन चुके हैं। उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वह प्रशासन और मीडिया — दोनों को खरीद लेता है।
आज मीडिया में “खनन” पर लिखना लगभग “खनन माफिया के खिलाफ खनन” जैसा हो गया है।
कई बड़े अखबारों में विज्ञापन से भरे पन्नों के नीचे सच्चाई दबा दी जाती है।
जो पत्रकार सच्चाई लिखते हैं, उन्हें या तो “ब्लैकमेलर” कहा जाता है या फिर “अंडर ऑब्जर्वेशन” में डाल दिया जाता है।
जनता जानती है कि हर रात दर्जनों ओवरलोड डंपर बिना चेकिंग के गुजरते हैं।
पुलिस चौकी से लेकर टोल गेट तक ‘सेटिंग’ का पूरा तंत्र चलता है।
किसी को रोकने की हिम्मत नहीं, क्योंकि “खनन” अब केवल पत्थर-रेत का व्यापार नहीं — बल्कि सत्ता और पैसों का गठबंधन बन चुका है।
नदियों का पर्यावरणीय ह्रास — एक वैज्ञानिक दृष्टि से,जब नदियों से अंधाधुंध रेत और पत्थर निकाले जाते हैं, तो तीन प्रमुख पर्यावरणीय नुकसान होते हैं:
- जलस्तर में गिरावट:
खनन से नदी तल नीचा हो जाता है, जिससे भूमिगत जलस्रोत कमजोर होते हैं। परिणामस्वरूप, गाँवों में कुएँ-स्रोत सूखने लगते हैं। - जैव विविधता पर असर:नदी किनारे के पेड़-पौधे, पक्षी और मछलियाँ अपने आवास खो देते हैं। कोसी और शारदा जैसी नदियों में मछलियों की कई प्रजातियाँ समाप्ति की कगार पर हैं।
- क्षरण और बाढ़ का खतरा:नदी के किनारों का कटाव बढ़ जाता है। बरसात के समय यह पानी पहाड़ों से वेग में उतरकर निचले इलाकों में तबाही मचाता है। जो कभी धीरे बहती नदियाँ थीं, अब रौद्र रूप धारण कर गाँव बहा ले जाती हैं। क्या आपदाओं की जड़ में खनन भी है?उत्तराखंड में हर साल आपदा आती है — पर सवाल यह है कि क्या यह केवल “प्राकृतिक” है?
या फिर हमने खुद पहाड़ों को इतनी चोटें दी हैं कि अब वह दर्द में चिल्ला रहे हैं?
जोशीमठ, धरासू, नैनीताल, बागेश्वर — सब जगह जमीन फट रही है।
भूगर्भ वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि “अंधाधुंध निर्माण और खनन” ने पहाड़ों की जल धारण क्षमता को खत्म कर दिया है।
पानी अब रिस नहीं पाता — वह सीधे बह जाता है, मिट्टी बहा ले जाता है, और घरों को खा जाता है।
यही वजह है कि 2024/ 25 की बरसात में हजारों घर तबाह हो गए।
कई गाँव अब “भूतिया गाँव” बन चुके हैं — जहां कभी जीवन था, अब केवल मलबा है।
अगर यही विकास है, तो विनाश कैसा होता होगा?
खनन के नाम पर राजनीतिक चमक?खनन अब केवल संसाधन नहीं, “राजनीतिक फंडिंग” का स्रोत बन चुका है।
टेंडर से लेकर ई-रवन्ना तक सब डिजिटल हो गया है — लेकिन रिश्वत और सेटिंग भी “डिजिटल” हो गई है।
जब किसी ट्रक पर खनन का “ई-टोकन” होता है, तो समझिए कि अवैध भी “वैध” बन जाता है।
राज्य के राजस्व में तो कुछ करोड़ आते हैं, पर पर्यावरण में जो क्षति होती है, उसका कोई मुआवजा नहीं।
यह वही उत्तराखंड है जहाँ एक समय कहा जाता था — “पहाड़ हमारे हैं, उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है।”
आज वही पहाड़ बिक रहे हैं, और बचाने वाले मौन हैं।
सरकार का सशक्त शासन मॉडल या खोखला ढांचा?मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने खनन के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं — ई-नीलामी, सैटेलाइट निगरानी, ई-रवन्ना जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं।
पर क्या यह पर्याप्त है?
यह तो ठीक वैसा है जैसे कोई रोगी कैंसर से ग्रस्त हो और उसे बुखार की गोली दी जाए।
नीतियाँ तभी प्रभावी होती हैं जब उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से हो — और ईमानदारी तब आती है जब भ्रष्टाचार पर अंकुश हो।
उत्तराखंड में आज स्थिति यह है कि अवैध खनन रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में सरकारी गाड़ियों के सामने होता है।
यह ‘सशक्त शासन मॉडल’ नहीं, बल्कि ‘मूक शासन मॉडल’ बन गया है।
विकास का संतुलन या विध्वंस की दौड़?उत्तराखंड की जनता अब दो हिस्सों में बँट गई है —
एक हिस्सा जो विकास की चमक देख रहा है,
और दूसरा हिस्सा जो उसी विकास की धूल में दबा जा रहा है।
खनन से राज्य को राजस्व मिलता है, पर क्या यह राजस्व उस प्रकृति की भरपाई कर सकता है जो सैकड़ों वर्षों में बनी थी?
क्या 100 करोड़ की केंद्रीय सहायता उन 1000 करोड़ की पर्यावरणीय क्षति को मिटा सकती है?
अब वक्त है सोचने का —
क्या हमें रेत निकालनी है या अपनी जड़ें?
क्या हमें डंपर चाहिए या पहाड़?
क्या हमें विकास चाहिए या जीवन?
उत्तराखंड के पहाड़ आज भी वही कह रहे हैं —
हमें सोना नहीं चाहिए, बस मिटने से बचा लो।”
खनन के पहाड़ तले दबता उत्तराखंड – विकास या विनाश की कहानी?”
✍️ लेखक: अवतार सिंह बिष्ट, संवाददाता — उत्तराखंड
कहते हैं, “धरती मां सब कुछ सह लेती है” — लेकिन शायद उत्तराखंड की धरती अब थक चुकी है। यहां विकास की परिभाषा अब पहाड़ काटने, नदियाँ सुखाने और ट्रकों में लदे कंक्रीट से मापी जाती है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘राज्य खनन तत्परता सूचकांक’ जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड को पंजाब और त्रिपुरा के साथ “सी कैटेगरी” में जगह मिली है। यानी, खनन सुधारों के क्षेत्र में राज्य ने कुछ अच्छा किया है — और इसके बदले 100 करोड़ रुपये का इनाम भी मिला है। सुनने में यह खबर किसी उपलब्धि जैसी लगती है, पर असलियत में यह ‘स्वर्ण पदक’ नहीं, बल्कि ‘मिट्टी में मिलते पहाड़ों का प्रमाणपत्र’ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि “खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस” को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब नदियाँ खून की तरह बह रही हैं, जब गाँव के गाँव दरक रहे हैं, जब पहाड़ों के पेट खाली हो रहे हैं — तो आखिर यह ‘सस्टेनेबिलिटी’ किसे कहते हैं?
खनन के नाम पर विनाश की गाथा?उत्तराखंड, जिसे कभी देवभूमि कहा जाता था, अब “डंपरभूमि” में बदल चुका है। खनन की नदियाँ अब देवप्रवाह नहीं रहीं, वे मलबे, डीज़ल और मशीनों की गंध से भर गई हैं।
गंगा की सहायक नदियाँ — कोसी, गौल, दुधिया, ढेला, डोभा, शरदापुर और शारदा — सभी से रेत और बजरी निकालने की होड़ लगी है। इन नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बिगड़ चुका है। पहले जो नदियाँ गर्जना करती थीं, अब वे कराह रही हैं। खनन ने उनका कलेजा खोद दिया है।
यह केवल पर्यावरणीय नुकसान नहीं, बल्कि सामाजिक त्रासदी भी है।
नदियों के किनारे बसे सैकड़ों गाँवों में जमीन धंसने लगी है।
घरों में दरारें हैं, खेतों में फटने लगी मिट्टी है, और पहाड़ों की गोद में भय है।
2023 और 2024 की बारिशों ने जो कहर बरपाया, वह किसी प्राकृतिक नहीं बल्कि “खनन प्रेरित आपदा” थी।
जब नदियों से अंधाधुंध खनन किया जाता है, तो उनकी धारा का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। इससे जल का दबाव बढ़ता है, कटाव तीव्र होता है, और बरसात के मौसम में नदियाँ अपने मार्ग से भटककर गाँवों, खेतों और सड़कों को निगल जाती हैं।
“खनन से विकास” का जो नारा है, वह अब “खनन से विनाश” में बदल चुका है।
कंक्रीट के जंगल और पहाड़ों की चुप्पी,कभी जिस उत्तराखंड की पहचान हरे भरे जंगलों और निर्मल नदियों से थी, अब वह कंक्रीट के पहाड़ों में बदल चुका है।
यह वही कंक्रीट है जो इन्हीं नदियों की रेत से निकली है।
पहाड़ों को काटकर होटल बनाए गए।
नदियों से बजरी निकालकर पुल और हाइवे बने।फिर इन्हीं हाइवे पर ओवरलोड डंपर चले — और उन्होंने सड़कों की सांसें उखाड़ दीं।
आज हालत यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़कों का डामर ओवरलोड डंपरों के नीचे पिघल चुका है। सड़कें जगह-जगह धंस चुकी हैं। गांव की गलियां टूटी हैं। हाईवे पर बने नए पुलों में दरारें पड़ी हैं।
और सबसे दुखद – इन ओवरलोड डंपरों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली।
कितनी ही दुर्घटनाएँ हुईं, लेकिन हर बार मामला “जांच जारी है” कहकर दबा दिया गया।
कभी किसी मंत्री का बयान आया, कभी किसी अधिकारी की “सख्त चेतावनी” — पर जमीनी हालात वही रहे।
ओवरलोड माफिया और मीडिया की मिलीभगत?खनन माफिया और ओवरलोड डंपर संचालक आज उत्तराखंड के सबसे ताकतवर “गैर-राजनीतिक नेता” बन चुके हैं। उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वह प्रशासन और मीडिया — दोनों को खरीद लेता है।
आज मीडिया में “खनन” पर लिखना लगभग “खनन माफिया के खिलाफ खनन” जैसा हो गया है।
कई बड़े अखबारों में विज्ञापन से भरे पन्नों के नीचे सच्चाई दबा दी जाती है।
जो पत्रकार सच्चाई लिखते हैं, उन्हें या तो “ब्लैकमेलर” कहा जाता है या फिर “अंडर ऑब्जर्वेशन” में डाल दिया जाता है।
जनता जानती है कि हर रात दर्जनों ओवरलोड डंपर बिना चेकिंग के गुजरते हैं।
पुलिस चौकी से लेकर टोल गेट तक ‘सेटिंग’ का पूरा तंत्र चलता है।
किसी को रोकने की हिम्मत नहीं, क्योंकि “खनन” अब केवल पत्थर-रेत का व्यापार नहीं — बल्कि सत्ता और पैसों का गठबंधन बन चुका है।
नदियों का पर्यावरणीय ह्रास — एक वैज्ञानिक दृष्टि से,जब नदियों से अंधाधुंध रेत और पत्थर निकाले जाते हैं, तो तीन प्रमुख पर्यावरणीय नुकसान होते हैं:
- जलस्तर में गिरावट:
खनन से नदी तल नीचा हो जाता है, जिससे भूमिगत जलस्रोत कमजोर होते हैं। परिणामस्वरूप, गाँवों में कुएँ-स्रोत सूखने लगते हैं। - जैव विविधता पर असर:नदी किनारे के पेड़-पौधे, पक्षी और मछलियाँ अपने आवास खो देते हैं। कोसी और शारदा जैसी नदियों में मछलियों की कई प्रजातियाँ समाप्ति की कगार पर हैं।
- क्षरण और बाढ़ का खतरा:नदी के किनारों का कटाव बढ़ जाता है। बरसात के समय यह पानी पहाड़ों से वेग में उतरकर निचले इलाकों में तबाही मचाता है। जो कभी धीरे बहती नदियाँ थीं, अब रौद्र रूप धारण कर गाँव बहा ले जाती हैं। क्या आपदाओं की जड़ में खनन भी है?उत्तराखंड में हर साल आपदा आती है — पर सवाल यह है कि क्या यह केवल “प्राकृतिक” है?
या फिर हमने खुद पहाड़ों को इतनी चोटें दी हैं कि अब वह दर्द में चिल्ला रहे हैं?
जोशीमठ, धरासू, नैनीताल, बागेश्वर — सब जगह जमीन फट रही है।
भूगर्भ वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि “अंधाधुंध निर्माण और खनन” ने पहाड़ों की जल धारण क्षमता को खत्म कर दिया है।
पानी अब रिस नहीं पाता — वह सीधे बह जाता है, मिट्टी बहा ले जाता है, और घरों को खा जाता है।
यही वजह है कि 2024 की बरसात में हजारों घर तबाह हो गए।
कई गाँव अब “भूतिया गाँव” बन चुके हैं — जहां कभी जीवन था, अब केवल मलबा है।
अगर यही विकास है, तो विनाश कैसा होता होगा?
खनन के नाम पर राजनीतिक चमक?खनन अब केवल संसाधन नहीं, “राजनीतिक फंडिंग” का स्रोत बन चुका है।
टेंडर से लेकर ई-रवन्ना तक सब डिजिटल हो गया है — लेकिन रिश्वत और सेटिंग भी “डिजिटल” हो गई है।
जब किसी ट्रक पर खनन का “ई-टोकन” होता है, तो समझिए कि अवैध भी “वैध” बन जाता है।
राज्य के राजस्व में तो कुछ करोड़ आते हैं, पर पर्यावरण में जो क्षति होती है, उसका कोई मुआवजा नहीं।
यह वही उत्तराखंड है जहाँ एक समय कहा जाता था — “पहाड़ हमारे हैं, उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है।”
आज वही पहाड़ बिक रहे हैं, और बचाने वाले मौन हैं।
सरकार का सशक्त शासन मॉडल या खोखला ढांचा?मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने खनन के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं — ई-नीलामी, सैटेलाइट निगरानी, ई-रवन्ना जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं।
पर क्या यह पर्याप्त है?
यह तो ठीक वैसा है जैसे कोई रोगी कैंसर से ग्रस्त हो और उसे बुखार की गोली दी जाए।
नीतियाँ तभी प्रभावी होती हैं जब उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से हो — और ईमानदारी तब आती है जब भ्रष्टाचार पर अंकुश हो।
उत्तराखंड में आज स्थिति यह है कि अवैध खनन रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में सरकारी गाड़ियों के सामने होता है।
यह ‘सशक्त शासन मॉडल’ नहीं, बल्कि ‘मूक शासन मॉडल’ बन गया है।
समापन – विकास का संतुलन या विध्वंस की दौड़?उत्तराखंड की जनता अब दो हिस्सों में बँट गई है —
एक हिस्सा जो विकास की चमक देख रहा है,
और दूसरा हिस्सा जो उसी विकास की धूल में दबा जा रहा है।
खनन से राज्य को राजस्व मिलता है, पर क्या यह राजस्व उस प्रकृति की भरपाई कर सकता है जो सैकड़ों वर्षों में बनी थी?
क्या 100 करोड़ की केंद्रीय सहायता उन 1000 करोड़ की पर्यावरणीय क्षति को मिटा सकती है?
अब वक्त है सोचने का —
क्या हमें रेत निकालनी है या अपनी जड़ें?
क्या हमें डंपर चाहिए या पहाड़?
क्या हमें विकास चाहिए या जीवन?
उत्तराखंड के पहाड़ आज भी वही कह रहे हैं —
हमें सोना नहीं चाहिए, बस मिटने से बचा लो।”
कहते हैं, “धरती मां सब कुछ सह लेती है” — लेकिन शायद उत्तराखंड की धरती अब थक चुकी है। यहां विकास की परिभाषा अब पहाड़ काटने, नदियाँ सुखाने और ट्रकों में लदे कंक्रीट से मापी जाती है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘राज्य खनन तत्परता सूचकांक’ जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड को पंजाब और त्रिपुरा के साथ “सी कैटेगरी” में जगह मिली है। यानी, खनन सुधारों के क्षेत्र में राज्य ने कुछ अच्छा किया है — और इसके बदले 100 करोड़ रुपये का इनाम भी मिला है। सुनने में यह खबर किसी उपलब्धि जैसी लगती है, पर असलियत में यह ‘स्वर्ण पदक’ नहीं, बल्कि ‘मिट्टी में मिलते पहाड़ों का प्रमाणपत्र’ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि “खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस” को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब नदियाँ खून की तरह बह रही हैं, जब गाँव के गाँव दरक रहे हैं, जब पहाड़ों के पेट खाली हो रहे हैं — तो आखिर यह ‘सस्टेनेबिलिटी’ किसे कहते हैं?
खनन के नाम पर विनाश की गाथा?उत्तराखंड, जिसे कभी देवभूमि कहा जाता था, अब “डंपरभूमि” में बदल चुका है। खनन की नदियाँ अब देवप्रवाह नहीं रहीं, वे मलबे, डीज़ल और मशीनों की गंध से भर गई हैं।
गंगा की सहायक नदियाँ — कोसी, गौल, दुधिया, ढेला, डोभा, शरदापुर और शारदा — सभी से रेत और बजरी निकालने की होड़ लगी है। इन नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बिगड़ चुका है। पहले जो नदियाँ गर्जना करती थीं, अब वे कराह रही हैं। खनन ने उनका कलेजा खोद दिया है।
यह केवल पर्यावरणीय नुकसान नहीं, बल्कि सामाजिक त्रासदी भी है।
नदियों के किनारे बसे सैकड़ों गाँवों में जमीन धंसने लगी है।
घरों में दरारें हैं, खेतों में फटने लगी मिट्टी है, और पहाड़ों की गोद में भय है।
2023 और 2024 की बारिशों ने जो कहर बरपाया, वह किसी प्राकृतिक नहीं बल्कि “खनन प्रेरित आपदा” थी।
जब नदियों से अंधाधुंध खनन किया जाता है, तो उनकी धारा का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। इससे जल का दबाव बढ़ता है, कटाव तीव्र होता है, और बरसात के मौसम में नदियाँ अपने मार्ग से भटककर गाँवों, खेतों और सड़कों को निगल जाती हैं।
“खनन से विकास” का जो नारा है, वह अब “खनन से विनाश” में बदल चुका है।
कंक्रीट के जंगल और पहाड़ों की चुप्पी,कभी जिस उत्तराखंड की पहचान हरे भरे जंगलों और निर्मल नदियों से थी, अब वह कंक्रीट के पहाड़ों में बदल चुका है।
यह वही कंक्रीट है जो इन्हीं नदियों की रेत से निकली है।
पहाड़ों को काटकर होटल बनाए गए।
नदियों से बजरी निकालकर पुल और हाइवे बने।फिर इन्हीं हाइवे पर ओवरलोड डंपर चले — और उन्होंने सड़कों की सांसें उखाड़ दीं।
आज हालत यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़कों का डामर ओवरलोड डंपरों के नीचे पिघल चुका है। सड़कें जगह-जगह धंस चुकी हैं। गांव की गलियां टूटी हैं। हाईवे पर बने नए पुलों में दरारें पड़ी हैं।
और सबसे दुखद – इन ओवरलोड डंपरों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली।
कितनी ही दुर्घटनाएँ हुईं, लेकिन हर बार मामला “जांच जारी है” कहकर दबा दिया गया।
कभी किसी मंत्री का बयान आया, कभी किसी अधिकारी की “सख्त चेतावनी” — पर जमीनी हालात वही रहे।
ओवरलोड माफिया और मीडिया की मिलीभगत?खनन माफिया और ओवरलोड डंपर संचालक आज उत्तराखंड के सबसे ताकतवर “गैर-राजनीतिक नेता” बन चुके हैं। उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वह प्रशासन और मीडिया — दोनों को खरीद लेता है।
आज मीडिया में “खनन” पर लिखना लगभग “खनन माफिया के खिलाफ खनन” जैसा हो गया है।
कई बड़े अखबारों में विज्ञापन से भरे पन्नों के नीचे सच्चाई दबा दी जाती है।
जो पत्रकार सच्चाई लिखते हैं, उन्हें या तो “ब्लैकमेलर” कहा जाता है या फिर “अंडर ऑब्जर्वेशन” में डाल दिया जाता है।
जनता जानती है कि हर रात दर्जनों ओवरलोड डंपर बिना चेकिंग के गुजरते हैं।
पुलिस चौकी से लेकर टोल गेट तक ‘सेटिंग’ का पूरा तंत्र चलता है।
किसी को रोकने की हिम्मत नहीं, क्योंकि “खनन” अब केवल पत्थर-रेत का व्यापार नहीं — बल्कि सत्ता और पैसों का गठबंधन बन चुका है।
नदियों का पर्यावरणीय ह्रास — एक वैज्ञानिक दृष्टि से,जब नदियों से अंधाधुंध रेत और पत्थर निकाले जाते हैं, तो तीन प्रमुख पर्यावरणीय नुकसान होते हैं:
- जलस्तर में गिरावट:
खनन से नदी तल नीचा हो जाता है, जिससे भूमिगत जलस्रोत कमजोर होते हैं। परिणामस्वरूप, गाँवों में कुएँ-स्रोत सूखने लगते हैं। - जैव विविधता पर असर:नदी किनारे के पेड़-पौधे, पक्षी और मछलियाँ अपने आवास खो देते हैं। कोसी और शारदा जैसी नदियों में मछलियों की कई प्रजातियाँ समाप्ति की कगार पर हैं।
- क्षरण और बाढ़ का खतरा:नदी के किनारों का कटाव बढ़ जाता है। बरसात के समय यह पानी पहाड़ों से वेग में उतरकर निचले इलाकों में तबाही मचाता है। जो कभी धीरे बहती नदियाँ थीं, अब रौद्र रूप धारण कर गाँव बहा ले जाती हैं। क्या आपदाओं की जड़ में खनन भी है?उत्तराखंड में हर साल आपदा आती है — पर सवाल यह है कि क्या यह केवल “प्राकृतिक” है?
या फिर हमने खुद पहाड़ों को इतनी चोटें दी हैं कि अब वह दर्द में चिल्ला रहे हैं?
जोशीमठ, धराली,धरासू, थराली चमोली मोपटा,नैनीताल, बागेश्वर — सब जगह जमीन फट रही है।
भूगर्भ वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि “अंधाधुंध निर्माण और खनन” ने पहाड़ों की जल धारण क्षमता को खत्म कर दिया है।
पानी अब रिस नहीं पाता — वह सीधे बह जाता है, मिट्टी बहा ले जाता है, और घरों को खा जाता है।
यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद केदारनाथ त्रासदी से शुरू हुआ या दौड़ आज भी ज़2024 /25की बरसात में हजारों घर तबाह हो गए।
कई गाँव अब “भूतिया गाँव” बन चुके हैं — जहां कभी जीवन था, अब केवल मलबा है।
अगर यही विकास है, तो विनाश कैसा होता होगा?
खनन के नाम पर राजनीतिक चमक?खनन अब केवल संसाधन नहीं, “राजनीतिक फंडिंग” का स्रोत बन चुका है।
टेंडर से लेकर ई-रवन्ना तक सब डिजिटल हो गया है — लेकिन रिश्वत और सेटिंग भी “डिजिटल” हो गई है।
जब किसी ट्रक पर खनन का “ई-टोकन” होता है, तो समझिए कि अवैध भी “वैध” बन जाता है।
राज्य के राजस्व में तो कुछ करोड़ आते हैं, पर पर्यावरण में जो क्षति होती है, उसका कोई मुआवजा नहीं।
यह वही उत्तराखंड है जहाँ एक समय कहा जाता था — “पहाड़ हमारे हैं, उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है।”
आज वही पहाड़ बिक रहे हैं, और बचाने वाले मौन हैं।
सरकार का सशक्त शासन मॉडल या खोखला ढांचा?मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने खनन के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं — ई-नीलामी, सैटेलाइट निगरानी, ई-रवन्ना जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं।
पर क्या यह पर्याप्त है?
यह तो ठीक वैसा है जैसे कोई रोगी कैंसर से ग्रस्त हो और उसे बुखार की गोली दी जाए।
नीतियाँ तभी प्रभावी होती हैं जब उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से हो — और ईमानदारी तब आती है जब भ्रष्टाचार पर अंकुश हो।
उत्तराखंड में आज स्थिति यह है कि अवैध खनन रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में सरकारी गाड़ियों के सामने होता है।
यह ‘सशक्त शासन मॉडल’ नहीं, बल्कि ‘मूक शासन मॉडल’ बन गया है।
समापन – विकास का संतुलन या विध्वंस की दौड़?उत्तराखंड की जनता अब दो हिस्सों में बँट गई है —
एक हिस्सा जो विकास की चमक देख रहा है,
और दूसरा हिस्सा जो उसी विकास की धूल में दबा जा रहा है।
खनन से राज्य को राजस्व मिलता है, पर क्या यह राजस्व उस प्रकृति की भरपाई कर सकता है जो सैकड़ों वर्षों में बनी थी?
क्या 100 करोड़ की केंद्रीय सहायता उन 1000 करोड़ की पर्यावरणीय क्षति को मिटा सकती है?
अब वक्त है सोचने का —
क्या हमें रेत निकालनी है या अपनी जड़ें?
क्या हमें डंपर चाहिए या पहाड़?
क्या हमें विकास चाहिए या जीवन?
उत्तराखंड के पहाड़ आज भी वही कह रहे हैं —
हमें सोना नहीं चाहिए, बस मिटने से बचा लो।”