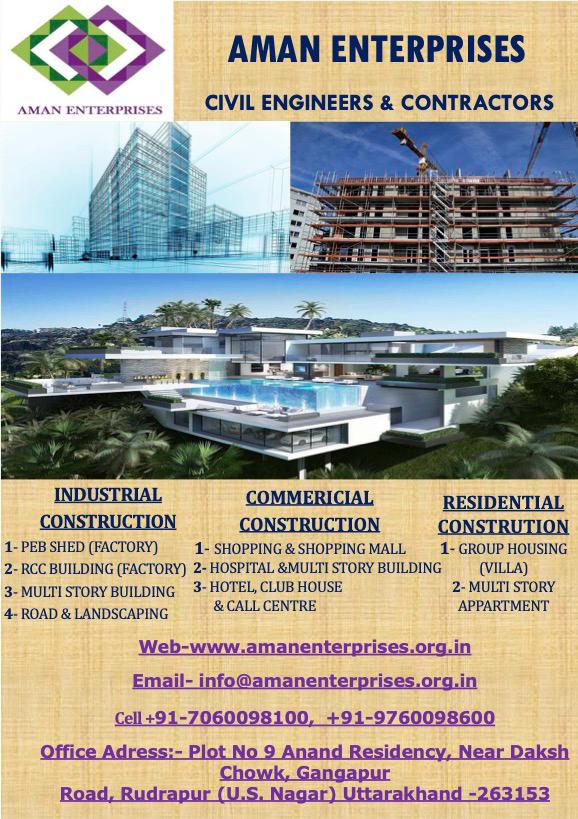भारतवर्ष में दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो हर क्षेत्र, हर समुदाय और हर व्यक्ति के जीवन में नई रोशनी भरती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ हिमालयी अंचलों — विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में — यह दिवाली पूरे देश से महीनेभर बाद मनाई जाती है? स्थानीय भाषा में इसे “बूढ़ी दिवाली” या “बग्वाल” कहा जाता है। यह परंपरा केवल एक तिथि का अंतर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जीवित एक सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के साथ सामंजस्य की प्रतीक परंपरा है।

✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
नामकरण की कथा और लोकमान्यता
बूढ़ी दिवाली के नामकरण के पीछे लोकविश्वास बड़ा रोचक है। कहा जाता है कि जब भगवान श्रीराम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे, तब हिमालय की पर्वतीय घाटियों में बसे जनजातीय समुदायों तक यह शुभ समाचार काफी देर से पहुँचा। कठिन पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संदेश पहुँचने में लगभग एक माह लग गया। जब यह सूचना वहाँ के लोगों को मिली, तब उन्होंने भी हर्षोल्लास में दीप प्रज्वलित कर दिवाली मनाई — और तभी से इस पर्व को “बूढ़ी दिवाली” कहा जाने लगा।
यह नाम न केवल एक ऐतिहासिक स्मृति है, बल्कि उस युग की संचार सीमाओं, भौगोलिक परिस्थितियों और मानवीय भावनाओं का प्रतीक भी है।
लोकसंस्कृति में गहराई से रचा-बसा पर्व
उत्तराखंड के जौनसार-बावर, टौंस घाटी, गढ़वाल के कुछ गाँवों और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली का आयोजन अत्यंत भव्यता से किया जाता है। इस उत्सव की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पटाखों की गूंज नहीं, बल्कि ढोल-दमाऊ की थाप सुनाई देती है।
भीमल की लकड़ी से बनी मशालें जलाकर ग्रामीण गाँव-गाँव में प्रकाश यात्रा निकालते हैं। इन मशालों की रोशनी में झैंता, हारुल, रासो और तांदी जैसे लोकनृत्यों की धुन पर पूरा गाँव झूम उठता है। महिलाएँ पारंपरिक वस्त्रों में सजती हैं, पुरुष अपने वाद्य लेकर लोकगीतों की मधुर लहरियों में पर्व को जीवंत करते हैं।
फसल और लोकजीवन से जुड़ी आस्था
बूढ़ी दिवाली केवल धार्मिक या पौराणिक कारणों से नहीं, बल्कि कृषि जीवन से भी गहराई से जुड़ी है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह पर्व अक्सर फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। उस समय खेत खाली होते हैं, अन्नागार भरे होते हैं, और ग्रामीण जीवन राहत की साँस लेता है। यह समय लोकजीवन में कृतज्ञता और प्रसन्नता का होता है — जब लोग देवताओं का धन्यवाद करते हैं और आने वाले वर्ष की समृद्धि की कामना करते हैं।
यही कारण है कि इस पर्व में प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण के प्रति सम्मान प्रमुख तत्व के रूप में झलकता है।
आधुनिकता के बीच एक पर्यावरण संदेश
जहाँ आधुनिक भारत में दीपावली अक्सर शोरगुल, प्रदूषण और दिखावे का माध्यम बन गई है, वहीं हिमालयी क्षेत्रों की बूढ़ी दिवाली सादगी, संतुलन और पर्यावरणीय चेतना का उदाहरण पेश करती है। यहाँ पटाखों की जगह मशालें जलती हैं, रासायनिक रंगों की जगह प्राकृतिक दीपक जगमगाते हैं, और विलासिता की जगह लोक-संवेदना का दीप प्रज्वलित होता है।
यह पर्व हमें सिखाता है कि रोशनी का अर्थ केवल विद्युत दीयों या पटाखों से नहीं, बल्कि मन के अंधकार को दूर करने से है।
सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है
आज जब शहरीकरण और तकनीकी विकास के नाम पर लोकपरंपराएँ विलुप्त होती जा रही हैं, तब बूढ़ी दिवाली जैसे पर्व हमारी सांस्कृतिक जड़ों की याद दिलाते हैं। यह पर्व हमें बताता है कि आधुनिकता में भी परंपरा की लौ बुझनी नहीं चाहिए। उत्तराखंड और हिमाचल की यह दिवाली हमें सिखाती है कि आनंद का सबसे सच्चा रूप प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीने में है।
सरकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं को चाहिए कि ऐसे लोकपर्वों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। स्कूलों में इन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हों ताकि नई पीढ़ी इन परंपराओं से जुड़ सके।
समापन विचार
बूढ़ी दिवाली केवल “देरी से मनाई जाने वाली दिवाली” नहीं है, बल्कि यह भारत के हिमालयी हृदय की लोक-संवेदना, सांस्कृतिक अस्मिता और पर्यावरण प्रेम की दिव्य अभिव्यक्ति है।
जब हम दीप जलाते हैं, तो वह केवल मिट्टी का दीपक नहीं होता — वह हमारी परंपरा, आस्था और मानवता की लौ होती है।
जौनसार-बावर और कुल्लू की यह बूढ़ी दिवाली हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची रोशनी वही है, जो समय, दूरी और सीमाओं से परे होकर भी मानवीय भावनाओं को प्रकाशित करती है।
क्या
– अवतार सिंह बिष्ट
संपादक, हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
रूद्रपुर, उत्तराखंड